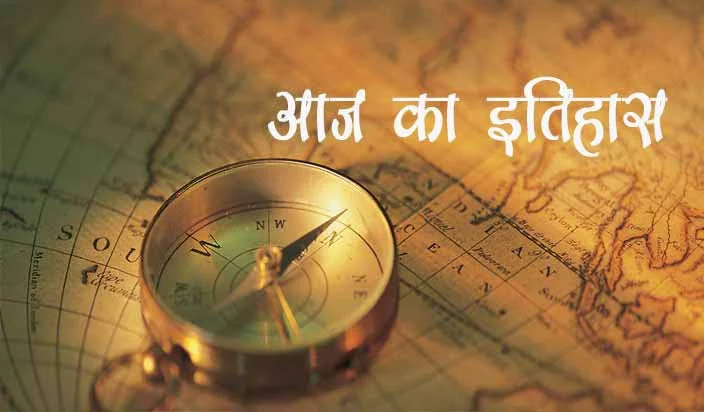आमतौर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आयात घटाना और निर्यात बढ़ाना जरूरी है। हर देश चाहता है कि उसकी सामग्री का दूसरे देश में निर्यात हो और उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अधिक आयात न करना पड़े। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर पिछले साल निजी महामारी से उथल-पुथल मचने के बाद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ा दिया है। पूंजी निवेश ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मांग बढ़ाने का काम बखूबी किया मगर यह भी माना गया था कि कभी न कभी निजी क्षेत्र निवेश का जिम्मा अपने हाथ में लेगा और वृद्धि बरकरार रहेगी। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.67 फीसदी था,जो 2024-25 में बढ़कर 3.4 फीसदी तक पहुंच गया। हालांकि महामारी से तो हम बहुत तेजी से उबर गए मगर निजी निवेश में इजाफा सुस्त ही रहा है। ध्यान रहे कि महामारी से पहले भी निजी निवेश धीमा ही था। महामारी के पहले के सालों में निवेश की स्थिति को कुछ हद तक बैलेंस शीट की दोहरी समस्या से भी समझा जा सकता है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद कंपनियों और बैंकों दोनों की बैलेंस शीट बहुत खस्ता हो गई थीं। हालांकि अब यह दिक्कत पूरी तरह दूर हो चुकी है और कंपनियों तथा बैंकों की बैलेंस शीट अच्छी स्थिति में है। किंतु निजी क्षेत्र अब भी ज्यादा निवेश करना नहीं चाहता। इस वित्त वर्ष में स्थिर मूल्यों पर देश का सकल स्थिर पूंजी निर्माण जीडीपी के 33.4 फीसदी के बराबर रहने का अनुमान है। लगातार ऊंची वृद्धि हासिल करने के लिए इसे बढावा देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी हफ्ते निजी कंपनियों से कहा कि उन्हें मूक दर्शक नहीं बने रहना है। उन्होंने कंपनियों से मौके पहचानने और चुनौतियां स्वीकारने के लिए कहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि निजी क्षेत्र को बताना चाहिए कि उन्हें निवेश बढ़ाने से क्या बात रोक रही है। सरकार बुनियादी ढांचा सुधारने के लिए भारी खर्च के साथ ही निवेश बढ़ाने के प्रयास भी कर रही है। उदाहरण के लिए 2014 के बाद से अब तक उसने 42,000 से अधिक नियम-कायदे हटा दिए हैं। 3,700 से अधिक कानूनी प्रावधानों को फौजदारी से बाहर कर दिया गया है और आगे भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। विनियमन आयोग पर चर्चा हो रही है। चूंकि वास्तव में निवेश राज्यों के भीतर होता है, इसलिए आयोग को अपने काम के दायरे के हिसाब से राज्यों के साथ मिलकर काम करना होगा। 2000 के दशक की तेज वृद्धि असल में 1990 के दशक के सुधारों के कारण आई थी। कुछ प्रस्तावित उपायों को कारोबारी सुगमता ब?ाने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा माना जा सकता है, जिनका फायदा आगे चलकर मिलेगा किंतु भारतीय कंपनियों के निवेश नहीं करने की कई वजह हो सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंक?े बताते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में 75 फीसदी क्षमता का इस्तेमाल हो रहा है, जो लंबे अरसे के औसत से कुछ ही ज्यादा है। आम तौर पर कंपनियां इसी स्तर से क्षमता बढ़ाने के लिए नया निवेश करने की सोचती हैं। लेकिन उनकी अनिच्छा की दो बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली, अनिश्चितता भरा वैश्विक माहौल, जिसमें डॉनल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद इजाफा ही हुआ है। दूसरी, चीन में आवश्यकता से अधिक क्षमता होना, जिसके कारण कंपनियों के लिए निर्यात बढ़ने की संभावना घट जाती है।2000 के दशक में अधिक निवेश के साथ ऊंची आर्थिक वृद्धि तो हो ही रही थी, निर्यात भी बहुत बढ़ रहा था। विश्व बैंक के आंकड़ोंके अनुसार जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी 2003 में 15 फीसदी थी, जो 2013 में बढ़कर 25 फीसदी से ऊपर चली गई। मगर 2019 में यह घटकर 18.7 फीसदी रह गई। उसके बाद से हिस्सेदारी बढ़ी है मगर अपने सर्वोच्च स्तर से बहुत कम है। निवेश और कुल वृद्धि में कमजोरी को निर्यात की सुस्ती से समझा जा सकता है। सरकार निर्यात पर शुल्क कम कर रही है मगर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
निर्यात में बढ़ोत्तरी जरूरी?